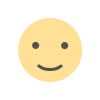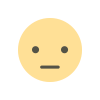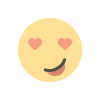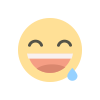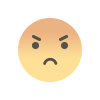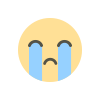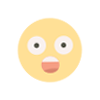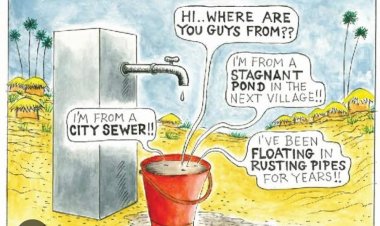करम पर्व : झारखंड की आत्मा और लोकगीतों की विरासत
झारखंड की मिट्टी और यहां की संस्कृति की आत्मा अगर किसी एक पर्व में सजीव होती है तो वह है करमा पूजा। भादो मास की एकादशी को मनाया जाने वाला यह पर्व केवल पूजा-अर्चना भर नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक चेतना, सामाजिक एकजुटता और प्रकृति के साथ अटूट रिश्ते का उत्सव है।

करमा सिर्फ़ आदिवासी समाज का नहीं, बल्कि झारखंड-बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और देश के कई हिस्सों में आदिवासी से लेकर सदान समुदाय तक सभी द्वारा मनाया जाने वाला सामूहिक उत्सव है। यह पर्व समाज की विविधता को एक सूत्र में पिरोता है और भाईचारे, प्रकृति-प्रेम तथा सामूहिकता का प्रतीक है।
झारखंड की मिट्टी और यहां की संस्कृति की आत्मा अगर किसी एक पर्व में सजीव होती है तो वह है करमा पूजा। भादो मास की एकादशी को मनाया जाने वाला यह पर्व केवल पूजा-अर्चना भर नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक चेतना, सामाजिक एकजुटता और प्रकृति के साथ अटूट रिश्ते का उत्सव है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि मनुष्य और प्रकृति एक-दूसरे के पूरक हैं, अगर प्रकृति सुरक्षित है तो जीवन सुरक्षित है।
करमा पर्व की विशेषता यह है कि इसमें न तो किसी मूर्ति की आवश्यकता होती है और न ही किसी भव्य मंदिर की। यह सीधा प्रकृति की पूजा है। करम डाली, मिट्टी, बीज, पानी और सूरज की किरणें ही इसके देवता हैं। यही कारण है कि करमा पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि जीवन-दर्शन है, जो कहता है “प्रकृति ही ईश्वर है।” झारखंडी परंपरा में करमा की शुरुआत तब से मानी जाती है जब इंसान ने खेती को अपना मुख्य जीवन-धर्म बनाया। यही कारण है कि करमा पर्व को कृषि और बीजों से जोड़कर देखा जाता है।
लोकमान्यता के अनुसार करमा और धरमा दो भाई थे। दोनों हमेशा साथ रहते और धर्म-कर्म में लीन रहते। लेकिन एक बार करमा ने क्रोध में आकर करम डाली का अपमान कर दिया। इसके बाद उसके जीवन में दुख-तकलीफ आने लगी। अंततः एक वृद्धा ने उसे समझाया कि यह सब करम देव के अपमान का परिणाम है। तब करमा ने पुनः करम डाली की पूजा की, और उसके जीवन में खुशियां लौट आयीं। यह कथा हमें यही सिखाती है कि कर्म और धर्म अलग नहीं हो सकते। धर्म बिना कर्म अधूरा है और कर्म बिना धर्म का कोई मूल्य नहीं। यही करमा का सबसे बड़ा संदेश है।
करमा पर्व का माहौल बनते ही कुंवारी लड़कियां तो घर पर रहकर इस पर्व को बड़े आनंद के साथ मनाती हैं, लेकिन इस बीच नवविवाहिताओं को विशेष तौर पर अपने मायके की याद आने लगती है। इसर दौरान उन्हें आस होती है कि अब उनके भाई लियावन कराने अवश्य आयेंगे। भाई भी पूरे सम्मान के साथ अपनी बहनों को ससुराल से मायके लाते हैं। बहनों की प्रतीक्षा और भावनाएँ करमा गीतों में झलकती हैं। बहनें राह देख देखकर गुनगुनाती है–
“बड़का हो भइया मति लेगे अइहा, कहाँ पावब पाकल पान हो...
मइझला हो भइया मति लेंगे अइहा, कहाँ पावब बांधल खसिया...
छोटका हो भइया तोहें चइल अईहा , कांदि-कांदि मांगभे विदाइ हो....
दीदी के कर दे विदाई हो, अरे हो……..”
गीत का भाव बड़ा मार्मिक है- बहन अपने बड़े और मँझले भाइयों को आने से मना करती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे जल्दी विदाई नहीं करा पाएंगे। लेकिन छोटे भाई के आने पर वह आश्वस्त होती है कि वह तो छोटा है, वह रो-धोकर भी अपनी बहन की विदाई करा लेगा, फिर वो मायके जाकर करमा पूजा कर सकेंगी । हालांकि अपना मायके नहीं जा पाने की दशा में ससुराल में भी करमा पूजा करने की मान्यताएं है।
इस पर्व में सात या नौ दिन पूर्व करमइतिन लोग नहा-धोकर गांव से दूर नदी-नाला से बांस के डाला में बालू उठाकर लाती हैं। उस डाला में गेहूं, जौ, चना, उरद, धान, कुरथी, मूंग आदि बीज बो दिये जाते हैं। अब इस डाला को प्रतिदिन पानी से सींचने और रखरखाव की जिम्मेदारी कुछ मुख्य करमइतिनों को दी जाती है, जिन्हें डलइतिन कहा जाता है। यह जावा डाला गांव के पाहन ( पुजारी ) या मुख्य डलइतिन के घर रखा जाता है। जावा डाली को रोज शाम को अखरा में लाकर सभी करमइतिन एकत्र होकर जावा डाली के चारों ओर गोल घेरा बनाकर गीत गाते हुए उसे जगाती हैं, जिसे ‘जावा जागा' गीत कहते हैं। दो-चार दिनों में जब बीज अंकुरित हो जाते हैं, तब उसमें हल्दी पानी का छिड़काव किया जाता है ताकि पौधा पीला और सुंदर दिखे। यही ' जावा फूल ' कहलाता है।
करम पूजा के दिन गांव के करमइतिनों के भाई या ग्राम के पाहन सुबह-सुबह नहा-धोकर जंगल जाते हैं और वहां से करम के एक ही वृक्ष की दो डालियाँ काटकर लाते हैं और ढोल-मांदर बजाते हुए, गीत-नृत्य करते हुए अखरा में गाड़ देते हैं जिसे ‘ करम गोसाई ’ कहा जाता है। फिर उन करम डालियों को फूलों और जगमगाती लाइटों से सजाया जाता है। रात को सभी उपवास की हुई करमइतिन साड़ी पहनकर पूजा की थाली में सभी सामग्री सजाती हैं और घी का दिया जलाकर प्रार्थना करती हैं। फिर करमइतिनें अपने भाई के कान में जावा फूल खोंसती हैं और हाथ में धागा बांधती है।
तब भाई से बुलवाया जाता है “केकर करम, केकर धरम?” और बहन गर्व से जवाब देती है- “आपन करम, भैयाक धरम।”
यह संवाद करमा पर्व की आत्मा है, जो कर्म और धर्म को अविभाज्य बताता है। जिसके बदले में भाई अपनी बहनों को उपहार और आजीवन साथ निभाने का वचन देते हैं। इसलिए करमा पर्व को भाई-बहन का पर्व भी कहा जाता है। अगले दिन सूर्योदय से पूर्व करम डाली को नदी या तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है।
करम पर्व में युवतियाँ केवल अपने भाई की ही नहीं, बल्कि पिता की लंबी उम्र और घर की सुख-शांति की भी प्रार्थना करती हैं। यह लोकभावना इन खोरठा गीतों में झलकती है-
“दिहो दिहो करम गोसाईं दिहो आशीष हो,
भइया बप्पा जिये हमर लाखों बरीस हो।”
और तब करम राजा मानो आशीर्वाद देते हैं-
“देलियो गे करमइतीन, देलियो आशीष गे,
भइया बप्पा जियतो लाखों बरीस गे।”
करमा को मनौती पर्व भी कहा जाता है। इस पर्व में वैसी विवाहिताएँ जिनकी शादी हो चुकी है लेकिन संतान नहीं हुआ है, जिन्हें स्थानीय बोली में डंगुवा बेटी-छऊवा कहा जाता है। वे करमा पूजा के दिन अपनी थाली में एक पुष्ट, सुडौल खीरा रखती हैं और करम राजा से प्रार्थना करती हैं कि उन्हें भी वैसा ही स्वस्थ और सुडौल बेटा मिले। वहीं, अविवाहित युवतियाँ जिनका कोई भाई नहीं होता है, वे करम राजा से सुंदर और स्नेही भाई की मनौती करती हैं, ताकि आने वाले समय में वे भी भाई की लंबी उम्र के लिए करमा पूजा कर सकें।
करमा पर्व बिना गीत-संगीत के अधूरा है। करमा गीतों में प्रकृति की सुंदरता, उसकी रचनात्मकता और मानव जीवन के उतार-चढ़ाव का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। जावा उठाने से लेकर करम डाली विसर्जन तक, हर चरण पर गीत गाए जाते हैं। जावा जगाने के गीत, करम काटने के गीत, फूल तोड़ने के गीत, विदाई गीत और विसर्जन गीत शामिल है।
विदाई के समय गाए जाने वाले खोरठा गीत अत्यंत मार्मिक होते हैं, जैसे-
“आज रे करम गोसाईं घरे दुआरे रे,
काल रे करम गोसाईं कांस नदी पारे रे।”“ जाहो जाहो करम गोसाईं जाहो ससुराल हो,
आवते भादर मास आनबो घुराय हो।”
इन दोनों गीतों में पूजा का भाव, विदाई की पीड़ा और पुनर्मिलन की आशा सब कुछ झलकती है।
आज जबकि डीजे और आधुनिक साधन करमा पूजा का हिस्सा बनते जा रहे हैं, पारंपरिक वाद्य यंत्र जैसे ढोल, मांदर, बांसुरी, तीरियो और टुहीला धीरे-धीरे गुम होते जा रहे हैं। सामूहिक अखड़ा संस्कृति, जहाँ मालिक से लेकर मजदूर सब साथ नाचते-गाते थे, अब मंच और दर्शक की रेखा में बँटने लगी है। करमा हमें यही सिखाता है कि अगर अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपने वाद्य को नहीं बचाया तो हमारी पहचान खो जाएगी।
करमा पर्व हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। यह भाई-बहन के अटूट प्रेम, माता - पिता की सेवा, संतान-सुख की आशा और समाज की एकजुटता का उत्सव है। जावा का हर अंकुर हमें याद दिलाता है कि जीवन नये सृजन की प्रक्रिया है, और करमा राजा का हर गीत यह सिखाता है कि बिना प्रकृति के कोई भी जीवन संभव नहीं। आज जब पूरी दुनिया आधुनिकता की चकाचौंध में अपनी जड़ों को भूल रही है, करमा पर्व हमें वापस हमारी मिट्टी, हमारे लोकगीत और हमारी सामूहिक संस्कृति से जोड़ता है। यही वजह है कि करमा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि झारखंड की आत्मा है।